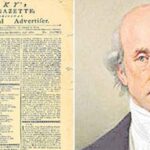बृज खंडेलवाल
___________
भारत ने आज़ादी के बाद अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा कर आर्थिक मोर्चे पर भारी कीमत चुकाई है। इसका बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी की गांधीवादी विचारधारा के प्रति एक दिखावटी प्रतिबद्धता, जिसने बार-बार लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी, इस उम्मीद में कि इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश की बजाय भारत “अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी” जैसे गांधीवादी आदर्शों से खेलता रहा और उन विशाल परियोजनाओं का उपहास उड़ाता रहा जो देश की तस्वीर बदल सकती थीं।
गांधीवादी मूल्यों की आड़ में हमने आधुनिक पश्चिमी सोच को खारिज किया और लाइसेंस राज व इंस्पेक्टर राज के ज़रिये तेज़ औद्योगीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया।
“छोटा सुंदर है” — यह सूत्र जिसे अक्सर अर्थशास्त्री ई.एफ. शूमाकर से जोड़ा जाता है और गांधीजी की आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना से मेल खाता है — लंबे समय से भारत की आर्थिक सोच को दिशा देता रहा है। लेकिन लघु उद्योगों, कुटीर इकाइयों और स्थानीय समाधानों पर यह भरोसा अब देश की प्रगति में बाधा बन गया है। असल में, आकार मायने रखता है — और पैमाने की अर्थव्यवस्था ऐसे नतीजे देती है जो छोटे प्रयास नहीं दे सकते।
जहां गांधीवादी सोच ग्रामीण भारत को सशक्त करने की चाह रखती थी, वहीं “छोटेपन” को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने आर्थिक रूप से बहुत कम फल दिए, जिससे साझा करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा। यदि भारत को विकास की ऊँचाई पर पहुँचना है तो उसे यह “लघु-प्रेम” छोड़कर बड़े और साहसिक विचारों को अपनाना होगा — जैसे चीन ने किया।
गांधीजी के आत्मनिर्भरता के स्वप्न ने खादी, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, खादी — दशकों की सब्सिडी के बावजूद यह उद्योग केवल 15 लाख लोगों को रोजगार देता है और भारत के GDP में 0.1% से भी कम योगदान करता है। इसके विपरीत, आईटी क्षेत्र — एक बड़े पैमाने का उद्योग — 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और लगभग 10% GDP में योगदान करता है।
लघु उद्योगों ने कई बार नकली, घटिया या अनधिकृत वस्तुएं ही बनाईं। ये सांस्कृतिक रूप से भले ही महत्वपूर्ण हों, लेकिन अक्सर संसाधनों को कम उत्पादकता वाले चक्रों में फंसा देते हैं, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते।
भारत का इंजीनियरिंग क्षेत्र भी यही कहानी कहता है। 1990 के दशक तक, अचार जैसे उत्पाद भी केवल लघु इकाइयों के लिए आरक्षित थे, जिससे विकास रुका। आज भारत में 6 करोड़ से अधिक SME हैं, लेकिन अधिकांश के पास पूंजी और तकनीक की कमी है, जिससे इनका उत्पादन सीमित ही रह जाता है।
दूसरी ओर, चीन ने बड़े पैमाने की सोच को अपनाकर चमत्कार कर दिखाया है। शेनझेन, जो कभी एक मछली पकड़ने वाला गांव था, आज वैश्विक निर्माण केंद्र है — स्मार्टफोन से लेकर कपड़े तक सब कुछ यहां बड़े पैमाने पर बनता है। यह बदलाव दर्शाता है कि अगर भारत भी “भावनाओं की जगह पैमाने को” महत्व देता, तो क्या संभव हो सकता था।
“छोटा सुंदर है” जैसी सोच ने भारत को मध्यम परिणामों के लिए तैयार कर दिया है और उच्च विकास की छलांग को टाल दिया है। भारत के विकेन्द्रित समाधान — जैसे सोलर माइक्रो ग्रिड — टिकाऊ तो हैं, लेकिन चीन की “थ्री गॉर्जेस डैम” जैसी परियोजनाओं जैसी आर्थिक ऊर्जा नहीं दे पाते।
भारत का इंफ्रा क्षेत्र भी यही कहानी बयां करता है। चीन ने जहां 2025 तक 40,000 किलोमीटर से अधिक हाई-स्पीड रेल और सड़क नेटवर्क तैयार कर लिया है, वहीं भारत की रेलवे प्रणाली अब भी आधुनिकता से पीछे है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं, जो अपेक्षाकृत “बड़ी सोच” का उदाहरण हैं, बार-बार टलती रही हैं।
चीन ने अपनी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू कर महाशक्ति का दर्जा पा लिया है, जबकि भारत की धीमी, टुकड़ों-टुकड़ों में बढ़ती सोच उसे पीछे धकेलती रहती है।
एक छोटे पाई (पाई = आर्थिक हिस्सेदारी) की उपमा यहाँ सटीक बैठती है। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $3,000 है, जबकि चीन की $14,000 से अधिक। छोटा आर्थिक आधार मतलब कम वेतन, कम निवेश और कम कल्याणकारी योजनाएं। भारत ने 2000 से अब तक 7 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई हैं, लेकिन अधिकांश केवल स्थानीय उपयोग के लिए बनी संकरी सड़कें हैं, न कि औद्योगिक कॉरिडोर।
बड़ी पाई, बड़े कदमों और उच्च जीवन स्तर की संभावना देती है — और भारत अब भी उस स्तर को पाने के लिए जूझ रहा है।
इतिहास में भारत का लाइसेंस राज (1947–1991) इस “छोटी सोच” का प्रतीक था, जिसमें छोटे उद्योग भी कागज़ी कार्यवाही में उलझे रहते और बड़े निजी उद्योगों को हतोत्साहित किया जाता। 1991 के आर्थिक सुधारों ने इस ढांचे को तोड़ा और इंफोसिस जैसी कंपनियों को जन्म दिया, लेकिन ये बदलाव अब भी अपवाद हैं।
वस्त्र उद्योग में भारत का हैंडलूम सेक्टर लाखों लोगों को रोज़गार देता है, लेकिन मजदूरी कम है और तकनीक पुरानी। वहीं चीन के ऑटोमेटेड कारखाने वैश्विक बाज़ार में छाए हुए हैं।
यह “प्रो-स्मॉल” वातावरण भारत को कम मूल्य वाले उत्पादन से चिपकाए रखता है।
निश्चित रूप से छोटे उद्योगों के फायदे हैं — भारत के SME क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और ये ग्रामीण संकट को थोड़ा सहारा देते हैं। फिर भी, बड़े स्तर की सोच को न अपनाने के कारण भारत ने 2008 के बाद के निर्माण-क्रांति के अवसर खो दिए।
मेगासिटीज़ और मेगाफैक्ट्रियां दिखाती हैं कि आकार परिणाम देता है। यदि भारत को विकास की छलांग लगानी है, तो उसे अपनी मानसिकता बदलनी होगी — छोटेपन के मोह से बाहर आकर बड़ी आर्थिक पाई या केक तैयार करनी होगी — जो ज़्यादा लोगों का पेट भर सके।