– डॉ. प्रियंका सौरभ
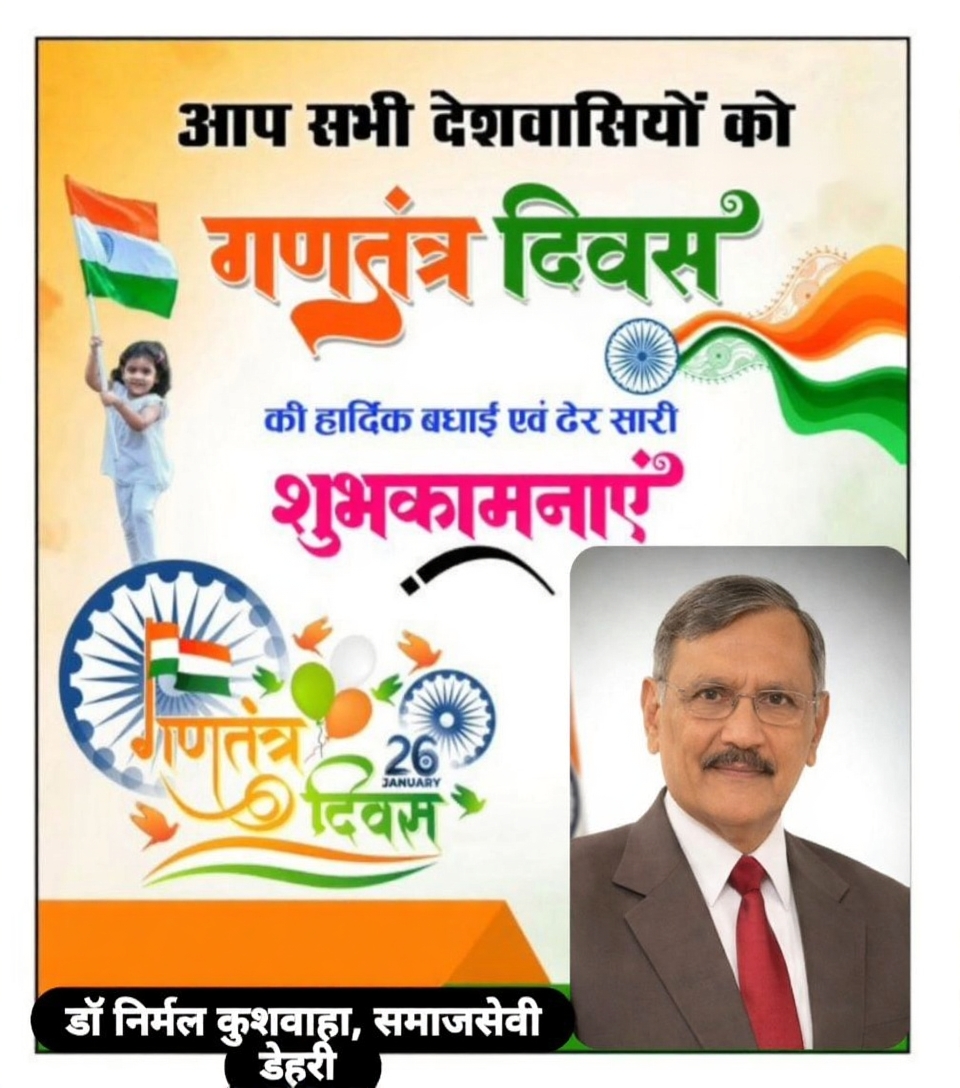
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और मासिक धर्म स्वच्छता को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है बल्कि यह भारतीय समाज की उस सामूहिक सोच को आईना दिखाते हैं, जिसमें आज भी मासिक धर्म को संकोच, चुप्पी और उपेक्षा के साथ देखा जाता है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि मासिक धर्म महज़ स्वास्थ्य या स्वच्छता का मुद्दा नहीं बल्कि गरिमा, समानता और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर संवैधानिक प्रश्न है।

भारत जैसे देश में जहाँ संविधान समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है, वहाँ लाखों छात्राओं का मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर होना व्यवस्था की गहरी विफलता को उजागर करता है। अदालत का यह हस्तक्षेप इसी विफलता को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम है। यह याद दिलाता है कि अधिकार केवल काग़ज़ों में दर्ज घोषणाएँ नहीं होते बल्कि उनका वास्तविक अर्थ तभी है, जब वे ज़मीनी हकीकत में दिखाई दें।
मासिक धर्म को लंबे समय तक केवल एक जैविक प्रक्रिया मानकर नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय या स्कूल प्रबंधन की सीमित जिम्मेदारी बनकर रह गया। सच्चाई यह है कि मासिक धर्म सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक स्तर पर गहरे प्रभाव डालता है। स्वच्छता सुविधाओं और सही जानकारी के अभाव में छात्राओं को न केवल संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है बल्कि शर्म और भय के कारण वे नियमित रूप से स्कूल आने से भी कतराने लगती हैं। कई मामलों में यह स्थिति स्थायी स्कूल ड्रॉपआउट का कारण बन जाती है।
अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि मासिक धर्म के दौरान उचित प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में किशोरियाँ हर महीने कई दिनों तक स्कूल नहीं जातीं। यह अनुपस्थिति धीरे-धीरे सीखने की प्रक्रिया को कमजोर करती है और अंततः शिक्षा से पूरी तरह कट जाने का जोखिम बढ़ा देती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या हम वास्तव में “सबके लिए शिक्षा” के लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं या यह केवल नीतिगत दस्तावेज़ों तक सीमित नारा बनकर रह गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।
जब स्कूलों में अलग और स्वच्छ शौचालय, साफ़ पानी, साबुन और सैनिटरी पैड जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं तो छात्राओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय जाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और गहरा करती है क्योंकि जहाँ लड़कों की शिक्षा बिना किसी जैविक बाधा के चलती रहती है, वहीं लड़कियों को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण पीछे धकेल दिया जाता है।
यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की भावना के विरुद्ध है, जो समानता और भेदभाव-रहित समाज की अवधारणा को आधार प्रदान करते हैं।
केवल अवसर की समानता पर्याप्त नहीं होती, जब तक उस अवसर तक पहुँचने के साधन भी समान न हों। मासिक धर्म स्वच्छता की अनदेखी करके हम अनजाने में ही लड़कियों को उस बराबरी से वंचित कर देते हैं, जिसका वादा संविधान करता है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं का अभाव महिलाओं और किशोरियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। जब किसी छात्रा को असुरक्षित और अवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने को मजबूर होना पड़े तो यह केवल स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि मानवीय गरिमा पर सीधा आघात है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं करता बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस धारणा को तोड़ता है कि सैनिटरी पैड या स्वच्छ शौचालय कोई “अतिरिक्त सुविधा” है। वास्तव में ये आवश्यक अधिकार है, जिनके बिना न तो स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है और न ही शिक्षा का अधिकार सार्थक हो सकता है। इस दृष्टि से अदालत का यह आदेश एक सामाजिक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
भारत में न्यायिक आदेशों की सबसे बड़ी चुनौती उनके प्रभावी क्रियान्वयन में दिखाई देती है। कई बार नीतियाँ और दिशा-निर्देश घोषणाओं और फाइलों तक सीमित रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यह निर्णय केवल अदालती आदेश या कानूनी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसका वास्तविक असर स्कूलों और छात्राओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए। सरकारी और निजी, शहरी और ग्रामीण-सभी स्कूलों में इन निर्देशों को समान रूप से लागू करना अनिवार्य है।
इस संदर्भ में निजी स्कूलों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अक्सर निजी शिक्षण संस्थान स्वयं को सरकारी योजनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग मान लेते हैं। अदालत का आदेश इस सोच को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और बताता है कि बच्चों के अधिकार के मामले में सरकारी और निजी का भेद स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि निजी स्कूल उच्च शुल्क वसूल सकते हैं तो वे छात्राओं की बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
यह स्वीकार करना होगा कि केवल आदेश और नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। जब तक समाज की सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक ऐसी पहल अधूरी ही रहेंगी। मासिक धर्म को लेकर फैली चुप्पी, अंधविश्वास और शर्म की भावना इस समस्या को और जटिल बनाती है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन केवल पैड वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जागरूकता, संवाद और वैज्ञानिक जानकारी को भी शिक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। लड़कों को भी इस चर्चा से अलग नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि संवेदनशील और समान समाज की नींव तभी पड़ती है, जब समझ साझा होती है।
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह आदेश केवल अनुपालन की बाध्यता नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। पर्याप्त बजट आवंटन, प्रभावी निगरानी तंत्र और स्पष्ट जवाबदेही तय किए बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती।
अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा यह स्पष्ट संकेत देती है कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता।
अंततः यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज की प्रगति का आकलन उसके सबसे कमजोर वर्ग के साथ किए गए व्यवहार से होता है। छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक सुविधाएँ देना कोई उपकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। अब असली परीक्षा यह है कि यह निर्णय काग़ज़ों से निकल कर ज़मीन पर उतरता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल स्कूलों की तस्वीर बदलेगा बल्कि उस सोच को भी बदलने की दिशा में निर्णायक कदम होगा, जो अब तक मासिक धर्म को अधिकार नहीं बल्कि बोझ समझती आई है।
(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
—————
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश






