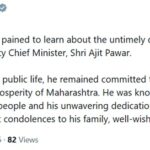क्या न्यायिक सक्रियता ने आगरा को बचाया है, या विकास को रोक रखा है?
____________
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पर्यावरणीय संकट से जूझता आगरा
__________
बृज खंडेलवाल
3 मई, 2025
___________
आगरा एक बार फिर उसी चौराहे पर खड़ा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को शहर के पर्यावरणीय संकटों को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है। अपने हालिया निर्देशों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी में गिरने वाले सभी नालों को चार महीनों के भीतर टैप करने और पेड़ों की कटाई पर बिना अनुमति रोक लगाने का आदेश दिया है।
लेकिन शीर्ष अदालत की न्यायिक सक्रियता को लेकर आगरा के व्यापारिक और औद्योगिक वर्गों में हमेशा से शंकाएं रही हैं। कई फैक्ट्री मालिकों और बिल्डरों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों की वजह से आगरा का “वर्ल्ड-क्लास” शहर बनने का सपना, जिसकी पहचान तरक्की और खुशहाली से होती, अधूरा रह गया है।
मगर अगर आगरा के पर्यावरणीय इतिहास पर नज़र डालें, तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) अथॉरिटी की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट की बार-बार की गई दख़लंदाज़ी, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता की जनहित याचिकाओं की वजह से संभव हुई, ने शायद आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद को एक भीषण पर्यावरणीय तबाही से बचा लिया।
1984 की शुरुआती जनहित याचिका में ताजमहल पर औद्योगिक धुएं, वाहनों के प्रदूषण और तेज़ाबी बारिश (एसिड रेन) के असर को गंभीर खतरा बताया गया था, जिसका मुख्य कारण सल्फर डाईऑक्साइड था। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना आए होते, तो TTZ क्षेत्र में मौजूद फाउंड्री, केमिकल प्लांट्स और खासतौर पर मथुरा रिफाइनरी जैसे उद्योग कोयला और कोक जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग जारी रखते, जिससे हवा और पानी दोनों की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती।
1996 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेशों के तहत न सिर्फ प्रदूषणकारी उद्योग बंद कराए गए बल्कि साफ़ ईंधन को अपनाना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना अनिवार्य किया गया।
कुछ लोगों का मानना है कि इन पाबंदियों के बिना आगरा को तात्कालिक औद्योगिक विकास ज़रूर मिलता, लेकिन लंबी अवधि में इसकी आर्थिक और पर्यावरणीय लागत बहुत ज़्यादा होती। सच तो यह है कि अगर TTZ और न्यायिक निगरानी नहीं होती, तो आगरा आज एक पिछड़ा हुआ, प्रदूषित शहर होता – अपनी विरासत और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता दोनों को खो चुका।
फिर भी यह हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के कई अहम निर्देश आज तक ज़मीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो सके। इसका बड़ा कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और अफसरशाही की सुस्ती है।
1993 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता की याचिका पर कार्रवाई की, तो डॉ. एस. वरदराजन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यापक उपाय सुझाए गए – जैसे वायु व जल प्रदूषण पर रोक, यमुना का पुनर्जीवन, पेड़ कटाई पर नियंत्रण, समुदाय तालाबों का पुनरुद्धार, धरोहर स्थलों का संरक्षण और उद्योगों पर कड़ी निगरानी।
एनवायरनमेंटलिस्ट डॉ देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं, “लेकिन तीन दशक बाद भी TTZ की स्थिति हमें बताती है कि ये सभी उपाय या तो लागू ही नहीं हुए या केवल दिखावे तक सीमित रहे। कोर्ट ने 292 प्रदूषणकारी उद्योगों को या तो स्थानांतरित करने या प्राकृतिक गैस जैसे साफ ईंधन पर लाने का आदेश दिया, कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाई, और धूल प्रदूषण रोकने के लिए हरित पट्टी विकसित करने को कहा। ताजमहल की नींव में नमी बनाए रखने के लिए यमुना में साल भर ताज़ा जल प्रवाह, नदी का गहरीकरण, मवेशियों की आवाजाही पर रोक, धोबीघाट और ताजगंज श्मशान जैसे प्रदूषणकारी गतिविधियों को हटाने का निर्देश भी दिया गया। यमुना बैराज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज सुधार जैसी अधोसंरचना परियोजनाएं भी प्रस्तावित की गईं।”
दुर्भाग्यवश, इन ज़रूरी उपायों पर या तो काम नहीं हुआ या बहुत ढीला-ढाला हुआ, जिससे कोई ठोस सुधार नहीं दिखता।
रिवर कनेक्ट कैंपेन से जुड़े सदस्यों की वेदना है कि यमुना नदी की दुर्दशा इस विफलता की प्रतीक बन गई है। बैराज परियोजना के लिए बजट आवंटन के बावजूद, यह अभी भी कागज़ों में अटका है। नदी में चमड़ा कतरनों, घरेलू कचरे और उद्योगों के ज़हरीले रसायनों के कारण जल का स्तर नगण्य है, और यह जानवरों के इस्तेमाल लायक भी नहीं बची। बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण अब भी जारी है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
यमुना किनारे चल रही ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ प्रदूषण नियमों की धज्जियाँ उड़ाती हैं, और ताजगंज श्मशान अब भी चालू है। वायु गुणवत्ता का हाल और भी गंभीर है – सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (SPM) स्तर अक्सर 350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर और गर्मियों में 600 तक पहुँच जाता है, जबकि मानक केवल 100 है।
TTZ में हरित क्षेत्र, जो बढ़ना चाहिए था, 6% से नीचे सिमट गया है, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 33% है। सामुदायिक तालाब गायब हो गए हैं और उनकी जगह कंक्रीट का जंगल उग आया है। आगरा के पश्चिमी हिस्से में वृक्षारोपण केवल फाइलों में सीमित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की कोई मजबूत निगरानी व्यवस्था नहीं है।
1999 में गठित TTZ अथॉरिटी के पास ना तो स्पष्ट कार्यदायित्व हैं और ना ही प्रभावी अधिकार, जिससे वह एक निष्क्रिय संस्था बनकर रह गई है। आगरा विकास प्राधिकरण और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे कई विभागों के आपसी समन्वय के अभाव में जवाबदेही खत्म हो गई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के नेक इरादों वाले आदेशों को पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से लागू किया गया होता, तो TTZ एक आदर्श पारिस्थितिक क्षेत्र बन सकता था – जहां विरासत संरक्षण और सतत विकास का संतुलन दुनिया को दिखाया जा सकता था।
मगर ये हो न सका, और आज ये आलम है कि शहर न हेरिटेज सिटी बन सका, न ही स्मार्ट सिटी।